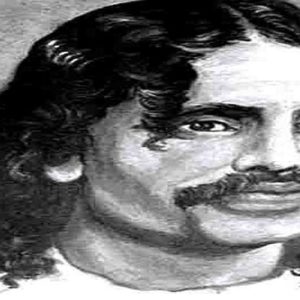‘तमस’ देश-विभाजन के पूर्व की हमारी सामाजिक मानसिकता और उसके अनिवार्य परिणाम के रूप में होने वाले भीषण साम्प्रदायिक दंगो की निर्मम करूण गाथा को चित्रित करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है. इसकी पृष्ठभूमि उस समय की है जब देश स्वतंत्रता के साथ विभाजन के दो राहे पर खड़ा था. अगर हम उस समय के ऐतिहासिक ग्रंथो और इतिहास की किताबों में साम्प्रदायिकता और विभाजन के दुःख, क्षोभ, निराशा, उजाड़पन और विभीषिका को देखने का प्रयास करेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी क्योंकि इन ग्रंथो में तत्कालीन राजनीतिक संवादों और विभाजन से प्रभावित लोगों का महज आकड़ा दिया गया है. यह तत्कालीन सामाजिक स्थिति और दुर्दशा को उचित रूप से कतई भी नहीं दर्शाता. जबकि साहित्यिक रचनाओं में हम विभाजन और उससे उपजे साम्प्रदायिक दंगों के मर्मपूर्ण चित्र को आसानी से देख और समझ पाते हैं और विभाजन की विभीषिका की मार्मिक छवि हमारे मानस पटल पर सहज ही उकर आती है. इन साहित्यिक रचनाओं में सआदत हसन मंटो की ‘ठंडागोश्त’, खुशवंत सिंह की ‘ट्रेन टू पाकिस्तान’, यशपाल का ‘झूठा सच’ आदि प्रमुख हैं.
इतिहासकार मुशीरुल हसन इस संबंध में लिखते हैं कि इन लेखकों ने धर्म को एक प्रमुख अवयव मानने से इनकार कर दिया और एकता को अनेकता पर तरजीह दी. इन लेखकों ने उन संयोजी और सहयोगी मूल्यों को उभारने की कोशिश की जिसे गंगा-जमुनी तहजीब कहते हैं और जो भारतीय समाज का एक प्रमुख गुण है, जिसे हम सदियों से जीते आए हैं.
‘तमस’ में भी भीष्म साहनी ने इन्हीं भारतीय मूल्यों को दिखाने की कोशिश की है और एक गैर-साम्प्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से यह बताने की कोशिश है कि भारतीय चाहें जिस भी धर्म और पंथ को मानने वाले हो उनकी पृष्ठभूमि एक ही हैं. लोग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते आए हैं. अंग्रेजो ने अपने ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति के तहत इस पारस्परिक निर्भरता और समान पृष्ठभूमि को तोड़ने की कोशिश की और साम्प्रदायिकता रुपी आग को हवा दी जिसका परिणाम अंततः विभाजन के रूप में देखने को मिला. 1947 के मार्च-अप्रैल महीने में पूरा पंजाब सम्प्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था. भीष्म सहनी ने ‘तमस’ में इन्ही भीषण साम्प्रदायिक दंगों की कहानी को वर्णित किया है,जो उनके गृह जिले रावलपिंडी में घटित हुई थी.
तमस की कहानी दो प्रमुख चरित्रों ‘मुराद अली’ और ‘नत्थू’ नामक चमार के वार्तालाप से शुरू होती है. मुराद अली, जो म्युनिसिपल कमेटी का एक कर्मचारी है, ‘नत्थू’ से एक अंग्रेज ‘सालेतरी साहब’ के भोजन के लिए एक सुअर को मारने को कहता है. नत्थू सूअर को मार देता है. लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उस मरे हुए सुअर को सालेतरी साहब ने नहीं खाया बल्कि उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया गया. इससे शहर में दंगा भड़क गया. सुअर मारने की त्वरित प्रतिक्रिया दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा गाय मारने से की गई. इससे दंगा शहर से लेकर आस-पास के गांवों तक फैल गया.
दंगों के बाद शहर के नागरिकों का एक शिष्टमंडल दल नगर में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर रिचर्ड से मिलता है लेकिन बिना किसी ठोस आश्वासन के लौट आता है. रिचर्ड के अनुसार यह महज एक ‘छोटी सी बात’ है. लेकिन शहर का माहौल एकदम इसके उलट है. शहर में लूट,हत्या और आगजनी का तांडव फैला हुआ है. सबसे विकराल घटना सैय्यदपुर गाँव में होती है,जहाँ के गुरूद्वारे में सारे सिख एकत्रित होकर मोर्चाबंदी करते है. वहीं मुसलमानों का मोर्चा शेख गुलाम रसूल के किले पर होता है. भीष्म साहनी कहते हैं ‘यह लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाइयों की श्रृंखला में महज एक कड़ी ही थी. लड़ने वालों के पांव बीसवी सदी में थे जबकि सर मध्ययुग में’. दरअसल भीष्म इन दंगो की ऐतिहासिकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं. वह इतिहास जिसे अंग्रेजों ने हमारे बीच में तोड़-मरोड़ कर पेश की और जिसके अनुसार मुसलमान तुर्क हैं और सिखों को खालसा सेना की तरह उनसे लोहा लेना है.
इसे भी पढ़ें- ओम फिनिशाय नमः महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के कप्तान नहीं लीडर हैं!
बहरहाल दो दिनों में सिखों का मोर्चा शिथिल पड़ने लगता है. सिखों का मोर्चा शिथिल होते देख जसबीर नामक सिक्ख महिला के नेतृत्व में तमाम सिख महिलाएं अपने बच्चों समेत कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं. यह घटना हमें उस ऐतिहासिक सच्चाई से परिचित कराती है जब ‘राज्य’ और ‘पुरुषों’ को हारता देख औरतें सती या जौहर कर अपने शरीर को त्याग देती हैं. पुरुषों के वर्चस्व की लड़ाई में भला इन महिलाओं का क्या ही दोष रहा होगा?
दंगों के पांच दिन बीत जाने के बाद दंगा शिथिल पड़ जाता है. लेकिन तब तक पूरे शहर का दृश्य ही बदला हुआ होता है. संपत्तियां लूट ली जाती हैं या जलकर खाक में मिला दी जाती हैं. हजारों लोग मारे जाते है या लापता हो जाते हैं और सदियों से विकसित मानवीय सभ्यता का एक क्षण में नाश हो जाता है.
इसके बाद दंगों के समाप्त होने की औपचारिकता घोषणा की जाती है. शहर में शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न पार्टियों और सम्प्रदायों के अग्रणी नेताओं के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन किया जाता है और शहर में शान्ति की अपील की जाती है. दिलचस्प बात ये है कि इनमे वे नेता भी शामिल होते हैं, जो दंगे भड़काने का प्रमुख कारण होते है. आम जनता तो इन दंगो का एक निमित्त मात्र होती है. वही मुराद अली जिसने सूअर को मारकर मस्जिद के सामने फेका था अब वह ‘हिन्दू-मुसलिम एकता’ के नारे लगा रहा होता है.
लोकल डिब्बा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें.
साम्प्रदायिकता के अतिरिक्त यह उपन्यास अंग्रेजों के कुटिल नीतियों, स्वार्थपरकता और तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं की आपसी खींचतान को भी उजागर करता है जिसके कारण स्वतंत्रता संघर्ष की धार कुंद पड़ रही थी. अगर हम भारतीय जनमानस की वर्तमान स्थिति को देखे तो पाते हैं कि भारत के जनमानस पर साम्प्रदायिकता अब भी उसी रूप में हावी है, जैसा कि 50 के दशक में था. यह एक अगम प्रश्न भी है कि अपनी तमाम अच्छाइयों के बाद भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें आखिर क्यों सफल नहीं हो पाती हैं?