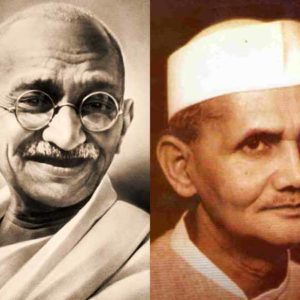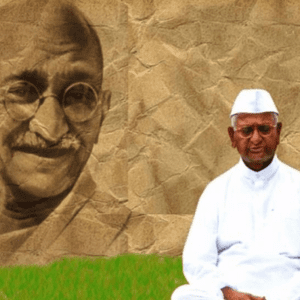कभी-कभी ऐसा होता है हम तृतीय श्रेणी के सिनेमाघर में बैठे होते हैं और कुछ देर शालीनता से बैठने के बाद, जब हमारे पैरों को थोड़े आराम की ज़रूरत महसूस होती है ,तो पैर सीधे करने का मन करता है और जब हम अपना पैर सीधा करते हैं तो अचानक से हमारा पैर अगली वाली सीट पर चला जाता है। तब हमारा शालीन स्वाभाव कहता है, “यह तो गलत है.”
अभी आपका शालीन स्वाभाव आपसे सही और गलत की बातें कर ही रहा होता है तब तक आपके पीछे वाली सीट से कुछ हलचल होती है आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं पीछे भी वही कहानी चल रही है. कोई आपकी सीट पर भी पैर चढ़ा आराम फ़रमा रहा है, तब यहीं होता है सोच का टकराव।
लोकल डिब्बा को फेसबुक पर लाइक करें
अब आपकी शालीनता दुबक के कहीं छिप जाती है और आप के अंदर एक नयी सोच पनपने लगती है और वो सोच ये होती है,”जब पीछे वाले आदमी ने ये काम किया तो मैं क्यों न करूँ”। बस यही एक शालीन सोच का क़त्ल हो जाता है जिम्मेदार आप ही होते है लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उस अवस्था मे वकील भी आप ही रहते हैं और जज भी आप ही।
मैंने सिनेमा घर वाली घटना का जिक्र क्यों किया क्योंकि हम जैसे युवाओं को अच्छे से समझ आ सके। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये तो एक छोटी सी घटना है, ऐसा अक्सर होता है। जब आप रेल यात्रा में हों या फिर कहीं भी, ये सोच अक्सर आ ही जाती है, जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो बात सिर्फ इतनी है, जिस सोच का आपने उस सिनेमाघर की सीट पे क़त्ल कर दिया, उसे फिर से जीवनदान दीजिये। उदार और विनम्र होना कोई बुरी बात नहीं, हमारी उदारता और विनम्रता एक आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग दे सकती है। उस सोच की मौत इस समाज को एक अंधकार की तरफ ले जा रही है, और हम युवा ही हैं जो अंधकार से उजाले का रास्ता जानते हैं।